
आज अपने ढंग के अकेले लेखक शैलेश मटियानी का जन्मदिन है। इस अवसर पर उनको याद कर रहे हैं वरिष्ठ लेखक प्रकाश मनु। इस आत्मीय संस्मरण को आप भी पढ़ सकते हैं-
===============================
[1]
मैं बहुत लेखकों से मिला हूँ। पर बहुत कम लेखक ऐसे मिले, जो पहली बार में ही छा जाते हैं और आप उनके साथ-साथ बहने लगते हैं। और आपका यह बहना जिंदगी भर रुकता नहीं है। वह आपके बस में ही नहीं होता। इसलिए कि उनका साथ किसी गाढ़े रस के झरने सा होता है। गहरा नशा! मटियानी जी ऐसे ही थे। उनसे जब पहली दफा मिला, तभी से उनका जादू मुझ पर तारी हो गया था।
‘हंस’ के दफ्तर में राजेंद्र यादव जी ने उनसे परिचय करवाया था, “आप जानते हैं इन्हें…? शैलेश मटियानी!” और वहाँ कुछ देर बातें हुई थीं, पर ऐसी बातें, जो दिल पर गहरे नक्श हो जाती हैं। वे चंद बातें अपनी मौज में जीने वाले हिंदी के सबसे औघड़ और फकीर लेखक सत्यार्थी जी को लेकर हुई थीं, तो फिर उनमें किस्से-कहानियों वाला पुट, अद्भुत-रस का मेल और मजेदारी न होती, यह भला कैसे हो सकता था? फिर लोकगीतों के ऐसे अलबेले मगर भुला दिए गए दरवेश पर मैंने किताब निकाली थी, यह खुद में किसी अजब किस्से-कहानी से कम न था। मटियानी जी को मैं शायद इसीलिए कुछ भा गया। और मैंने तो मटियानी जी को इतना पढ़ा था कि उन सरीखे उस्ताद किस्सागो से बतिया लेना ही मेरे लिए किसी गाढ़े नशे या सरूर से कम न था।
बातों-बातों में उन्होंने पूछा, “आप कहाँ हैं?” और जब मैंने हिंदुस्तान टाइम्स की पत्रिका ‘नंदन’ का जिक्र किया, तो बोले, “मैं कभी आऊँगा। आप पुस्तक की एक प्रति मेरे लिए रख लें।”
मटियानी जी ने कहा और मैंने सुन लिया—परम आनंद भाव से। पर वे आएँगे मुझ जैसे मामूली लेखक से मिलने, मेरे लिए तो यह कल्पना ही मुश्किल थी। लगभग असंभव! पर वे आए अपने लहीम-शहीम व्यक्तित्व और अपार जिंदादिली के साथ और उस पहली खुली मुलाकात में ही इतनी ढेर-ढेर सी बातें हुईं कि बरसों बाद भी वह रसमग्न कर देने वाली पूरी फिल्म मैं दिल के परदे पर फिर से देख सकता हूँ, जिसमें मटियानी जी की निजी जिंदगी के बेढब सफर, विलक्षण लेखकीय शक्सियत और अजीबोगरीब जिदों से लेकर दुनिया-जहान की बातें हुई थीं और मैं भूल गया था कि दफ्तर बंद होने के बाद मुझे घर भी जाना है।
मटियानी जी दीर्घसूत्री हैं, मगर अपन राम भी क्या कुछ कम हैं! अलबत्ता जब बातों के आसमान में उन्मुक्त उड़ानें भरते बहुत देर हो गई तो मटियानी जी ने हलके से डाँटा, “सिर्फ बातें ही करते रहोगे या चाय भी पिलाओगे?”
“ओह, चाय…!” मैं बड़ा शरमिंदा हुआ।
अभी तक तो उनके साथ जुड़ी तमाम-तमाम बातों, उत्तेजक बहसों, गोष्ठी-समारोहों और अखबारी पन्नों पर उनकी ‘युद्धं देहि’ वाली मुद्रा के हलचल भरे प्रसंगों और किस्म-किस्म के अद्भुत रस वाले किस्से-कहानियों से गुजरता हुआ मैं भूल ही गया था मैं भी इसी धरती का प्राणी हूँ और धरती के प्राणी जब देर तक काम या बातें करते-करते थक जाते हैं तो चाय भी पीते हैं।
अलबत्ता चाय आई और मस्ती से गपशप, ठहाकों पर ठहाके लगाते हुए चाय पी गई और चाय की चुस्कियों के साथ फिर जैसा कि होना ही था, साहित्य की किस्से-कहानियों से भी बढ़कर रंग और रसमयी दुनिया के चरचे और चरखे चल निकले। लगा कि मटियानी जी के साथ मैं एक अंतहीन साहित्यिक सफर में हूँ।
अजब सुरूर से भरा दिन था, जब साहित्य किताबों और कागजों से निकलकर खून में दौड़ने लगा था। और मुझे गालिब याद आने लगे थे, “रगों में दौड़ने-फिरने के हम नहीं काइल, जब आँख ही से न टपके तो लहू क्या है…”
उस दिन मटियानी गए तो ऐसा गहरा नशा छोड़कर कि सच्ची कहूँ तो आज तक वह उतरा नहीं है और हर दिन उसका रस कुछ और गहरा ही होता जाता है।
[2]
खैर, उस दिन तो जैसे-तैसे घर पहुँचा, पर फिर हफ्ते-दस दिन बाद मटियानी जी फिर मौजूद और पिछली बार से लेकर अब तक जो कुछ गुजरा, अपनी जीवन-कथा का हरफ-हरफ बता देने को इस कदर आतुर कि मैं फिर भूल गया कि एक दफ्तर भी होता है और उसका बंद होने का समय भी होता है।
जब दरबान ने बार-बार संकेत से सूचना दी कि गेट बंद करने का समय हो गया है और मैंने नहीं समझा, या कहिए कि जान-बूझकर नहीं समझना चाहा—तो उसने आकर बेशरमी से साफ-साफ ही कहा कि “सर, अब मुझे अपना काम करने दें, आप अपना करें।”
बेमन से मैंने बस्ता उठाया, मटियानी जी ने अपना बैग और हमारे कदम कैंटीन की ओर बढ़ चले, जिसके बंद होने का कोई चक्कर नहीं था।
मगर जब बातों में से बातों के ऐसे सुर निकले कि चारों ओर गहरा अँधेरा सा पसर गया, तो मुझे घर याद आया। फरीदाबाद की आखिरी गाड़ी के छूटने में कुछ ही समय था। “मटियानी जी अब तो मुश्किल…!” मैंने लाचारी से कहा। मेरे चेहरे पर अब एक घरेलू प्राणी के भय की दस्तक थी। और फिर मैं और मटियानी जी उठे, बेमन से।
मटियानी जी ने ऑटो पकड़ा और मैं जैसे-तैसे भागते-दौड़ते स्टेशन पहुँचा तो पता चला कि आखिरी गाड़ी निकल चुकी है। अब टुकड़ों-टुकड़ों में कई बसें पकड़कर घर जाना था। और चूँकि उस समय मोबाइल तो छोड़िए, फोन तक भी न था तो मन में विचारों का यह अंधड़ लग चल निकला कि ओह, घर पर सुनीता परेशान होगी।
मुझे पता था कि रात को देर होने पर उसे बस एक ही खयाल आता है कि मैं कहीं दुर्घटनागस्त होकर सड़क पर पड़ा हूँ…और मेरे चारों तरफ रोशनियाँ उगलती गाड़ियाँ भागी जा रही हैं। उसे लगता है, मेरे जैसे लापरवाह का और भला हो भी क्या सकता है? और यहाँ तक कि सही-सलामत घर आ जाने पर भी उसे विश्वास नहीं होता कि मैं ठीक-ठाक हूँ और बड़ी देर बाद वह सहज हो पाती है।
पर गनीमत यही कि खतरे की घंटी देख, घर आते ही मैंने मटियानी जी के एक से एक दिलचस्प किस्से छेड़े तो उसे सहज होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा।
[3]
मगर अब यह जल्दी-जल्दी होने लगा। बीच में मटियानी जी ने मेरे दो इंटरव्यू पढ़ लिए। एक में डा. रामविलास शर्मा से लंबी बातचीत थी और दूसरे में कमलेश्वर से। बस, मटियानी जी मेरे इंटरव्यूज के कुछ ऐसे कायल हो गए कि उन्हें लगा, ऐसे इंटरव्यू तो पूरे हिंदी साहित्य में कोई और नहीं कर सकता।
एक दिन आए तो बातों-बातों में बोले, “मनु, मैं तुम्हें इंटरव्यू दूँगा। बरसों पहले कमलेश्वर ने ‘सारिका’ से एक लेखक को भेजा था। वे भले सज्जन थे, मेरे घर बहुत दिन डेरा डाले रहे। पर इंटरव्यू देने का मूड नहीं बना।…मैंने तुम्हारे इंटरव्यू पढ़े हैं, तुम इंटरव्यू अच्छा लेते हो। थोड़ी फुरसत मिले तो मैं पूरा एक हफ्ता तुम्हारे घर आकर रुकूँगा। सात दिन हम सात विषय तय करके उस पर बात करेंगे। पूरी बातचीत रिकार्ड होगी। फिर वह किताब की शक्ल में आएगी। उस पर दोनों का नाम जाएगा। और हाँ—रॉयल्टी आधी-आधी!”
अब मुई रॉयल्टी की तो मुझे क्या परवाह थी? वे आधी नहीं, भले ही पूरी ले लें। पर हाँ, उनकी जो अफरातफरी वाली हालत थी, जिसमें मैं हमेशा उन्हें कहीं न कहीं तेजी में आते-जाते, बल्कि कहना चाहिए, भागते ही देखता था और भागते-भागते ही हमारी बातें होती थीं, उसमें यकीन नहीं आता था कि पूरा एक हफ्ता वे हमारे घर आकर रुकेंगे और बात हो पाएगी।
तो फिर मैंने तरीका यह निकाला कि हर बार जब वे आते तो मैं उनकी जीवन-कथा का कोई खास प्रसंग छेड़ देता और मटियानी जी लीन होकर सुनाते तो मैं मन के टेप पर पूरी बातचीत रिकार्ड कर लेता और दिन में कई-कई बार रिवाइंड करके पक्का करता जाता।
इस बीच मटियानी जी अपनी सारी नई-पुरानी किताबें मुझे दे गए। कुछ अरसा पहले उन्होंने ‘विकल्प’ और ‘जनपक्ष’ पत्रिकाएँ निकाली थीं, जिनकी खासी धूम रही थी। उनकी पुरानी फाइलें भी मुझे देना वे नहीं भूले। और यही नहीं, अपने जीवन में घटी एक से एक छोटी-बड़ी बात भी जैसे वे मुझे बता देना चाहते थे। पता नहीं, कैसे उन्हें यकीन हो गया था कि जो कुछ वे मुझे बता देंगे, वह रह जाएगा और कहीं न कहीं दर्ज होगा। उनकी अनकही कहानी अनकही न रहेगी।
उधर मटियानी जी के जीवन में पिछले कुछ बरसों में ऐसी भागमभाग थी, जिसे ठीक-ठीक समझना किसी के लिए भी मुश्किल था। मैं कुछ-कुछ अंदाजा लगा पा रहा था। लेकिन मैंने उन्हें पूरी तरह समझ लिया था, यह तो कैसे कहूँ? वे लगभग बदहवास हो चले थे। पूछने पर हमेशा उनका एक ही जवाब मिलता, “मनु, मैं जीवित कैसे हूँ, यह खुद मेरी समझ में नहीं आता। कायदे से तो जो परिस्थितियाँ हैं, उनमें मुझे जीवित नहीं होना चाहिए था!…”
सुनकर जी धक से रह जाता।
और फिर एक के बाद एक हादसे। उनमें सबसे घातक और मर्मांतक घटना थी, उनके पुत्र की क्रूरतापूर्ण हत्या। जैसे देखते ही देखते उनके जीवन में प्रलय आ गई हो। कुछ दिनों बाद मटियानी दिल्ली आए तो उन्होंने मुझे दरियागंज में किसी जगह बुलाया। पूरे एक घंटे वे मेरे सामने बैठे रहे। न उन्होंने कुछ कहा, न मुझसे कुछ कहा गया। फिर बोले, “मनु, अब तुम जाओ। आज मैं कुछ बात नहीं कर पाऊँगा।”
इस बीच उनके आर्थिक कष्ट और बढ़े ही! कुछ समय बाद केड़िया का एक लाख रुपए का पुरस्कार उन्हें मिला, तो यह खुशी थी कि आंशिक रूप से ही सही, अब उनके आर्थिक कष्टों का कुछ अंत होगा। लेकिन इसके साथ ही जो खबर मिली, वह कलेजा चीर देने वाली थी। पता चला कि मटियानी जी विक्षिप्त हो चुके हैं, इसलिए खुद पुरस्कार लेने भी नहीं आ सके!…
सुनकर मैं सन्न रह गया। हा हंत! मटियानी जी की यह हालत? इस आदमी के दारुण कष्टों का कोई अंत नहीं। साहित्य की तिकड़में भिड़ाने वालों को निराला के बाद इलाहाबाद में ही यह दूसरा एक बड़ा शिकार मिल गया? लगा कि अब तो उनसे मिल पाना भी शायद मुश्किल होगा। कभी बात हो सकेगी, इसका तो कतई यकीन ही नहीं था। और जाने कब से आगे खिसकते जा रहे इंटरव्यू की बात तो अब सोची भी नहीं जा सकती थी।…असंभव!
मेरे जीवन के ये सबसे दुखी और उजाड़ दिन थे। और इन्हीं दुखी और उजाड़ दिनों में अचानक फिर फोन पर मटियानी जी की की लरजती हुई आवाज, “मनु मैं मटियानी बोल रहा हूँ।”
यह तीन अक्तूबर, 1996 की बात है, जब कोई सवा साल के एक लंबे और दाहपूर्ण अंतराल के बाद चिर परिचित लहजे में मटियानी जी का फोन आया, “मनु, मैं मटियानी बोल रहा हूँ…!” सुनते ही जैसे मैं सुख-दुख की एक अजीब लहर में समा गया।
“अरे, मटियानी जी आप…? आप मटियानी जी, ठीक हैं ना!” मुझे यकीन नहीं हो रहा था मटियानी कैसे हो सकते हैं? उनके बारे में तो यह-वह और न जाने क्या-क्या कहा जा रहा है। तो फिर…?
डरते-डरते उनसे मिलने गया तो उनकी बातचीत या व्यवहार में मुझे कहीं कोई असमान्यता नहीं दिखाई दी। न कहीं स्मृति-लोप, न भाषा की असावधानी, न किसी और तरह की असामान्यता।
पता चला कि वे पिछले एक महीने से इलाज के लिए गोविंदबल्लभ पंत हॉस्पीटल में हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने बारीक से बारीक विवरण के साथ पिछले सवा साल की यातनाओं का पूरा वृत्तांत सुनाया। यह इतना दर्दनाक और एक साथ ही इतना मुकम्मल था कि मैं एकदम हिल गया।
इसके बाद तो अस्पताल में ही उनसे कई मुलाकातें हुईं। अपनी गहरी मानसिक यातनाओं के बावजूद हर दफा वे मुझे सजग और सचेत लगे। यहाँ तक मेरे आग्रह पर उन्होंने डायरी के पन्ने लिखने शुरू किए और उन्नीस पन्ने लिखे भी। एक दिन उन्होंने हल्द्वानी आने का निमंत्रण दिया। बोले, “चाहो तो मनु, तुम अब वह इंटरव्यू ले सकते हो।” और इस बात के लिए मान गए कि मैं चाहूँ तो अस्पताल में भी बातचीत हो सकती है।
यों भी अस्पताल में उनसे लगातार मिलते हुए एक महीना हो गया था और महीने भर में टुकड़ों-टुकड़ों में इतनी बातें हुई थी कि आगे की बातचीत के लिए कुछ-कुछ भूमिका बन गई थी।
[4]
मैं स्वीकार करूँगा कि 3 नवंबर, 1996 को शैलेंद्र चौहान के साथ फरीदाबाद से उनका इंटरव्यू लेने के लिए जाते समय मन थोड़ा डरा हुआ था कि न जाने बात हो भी पाएगी या नहीं? रमेश तैलंग को दिल्ली से सीधा पहुँचना था और वे बिल्कुल सही समय पर आए भी। पर मैं खुद आशंकित था। डरा-डरा। बार-बार सोच रहा था कि सवाल सुनकर मटियानी जी असहज या उत्तेजित तो नहीं हो जाएँगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटरव्यू ढंग का न बन पाए…या उनके भीतर की तकलीफें उसमें न आ सकें और पढ़ने वालों को यह बुरी तरह निराश करे?
लेकिन आश्चर्य! शुरुआती हिचकिचाहट और थोड़ी-सी ‘नर्वसनेस’ के बावजूद मटियानी जी ने इतने धीरज के साथ कोई चार घंटे तक सवालों के जवाब दिए और वे जवाब इतने अच्छे, सटीक और मुकम्मल थे कि हम लोग पूरे समय एक अजीब सी भावदशा में रहे। ऐसे सवाल भी जिन्हें पूछते हुए शुरू में हम डर रहे थे, पूछे गए और मटियानी जी ने बड़ी आसानी और सहजता से उन्हें झेला और लगभग निरुत्तर कर देने वाले जवाब दिए।
बातचीत की शुरुआत उनकी लेखन-यात्रा से हुई। मटियानी जी को कहानियाँ लिखते हुए कोई चार दशक हो गए थे। एक बड़ी और समृद्ध सृजन-यात्रा, जिस पर किसी को भी गर्व हो सकता है। मैंने जानना चाहा कि इतनी लंबी कथा-यात्रा के बाद वे कैसा महसूस करते हैं? अपने लेखन से वे कितने संतुष्ट हैं, कितने असंतुष्ट…?
सवाल सुनकर मटियानी जी के चेहरे पर थोड़ी हिचकिचाहट नजर आई। उनके स्वर में भी। उन्होंने इस बातचीत को आगे टालने के लिए कहा, “मनु, एक लंबी और हौलनाक बीमारी के बाद जिसमें अकथनीय यंत्रणा और तकलीफें मैंने सही है, आपके इस सवाल का जवाब देना मुझे मुश्किल लग रहा है…!” उनका वाक्य बीच में अधूरा टूट जाता है।
कुछ देर बाद उनकी ओर से एक अजीब सी पेशकश हुई, “क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग सवाल मुझे लिखकर दे दें, मैं उनके जवाब आपको लिखकर दे दूँगा! उसमें मुझे आसानी रहेगी और शायद बात भी पूरी तरह…!”
लेकिन मैं तो ऐसे किसी इंटरव्यू के लिए कतई तैयार नहीं था। ऐसे यांत्रिक इंटरव्यू में भला बातचीत की स्वाभाविक ऊष्मा कहाँ से आ सकती थी? कुछ सोचकर मैंने कहा, “अच्छा मटियानी जी, आप यही समझ लें कि इंटरव्यू तो यों ही हो रहा है।…आपसे नहीं बनेगा तो इसे आप निरस्त समझिए और फिर आप वाला ढंग ही अपना लेंगे।”
मटियानी जी मान गए। “ठीक है, जैसी आपकी इच्छा…!” कहकर अंतत: उन्होंने हथियार डाल दिए।
“अच्छा मटियानी जी, एक बात बताएँ। जो सवाल आपसे पूछा है कि आप अपने लेखन से कितने संतुष्ट, कितने असंतुष्ट हैं, अगर यह कुछ साल पहले आपसे पूछा जाता तो..?” मैंने अपने प्रश्न को थोड़े भिन्न ढंग से उनके आगे रखा।
मटियानी जी ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, “हो सकता है कि तब, यानी आज से पाँच-छह साल पहले मैं इसका जवाब दे पाता। लेकिन अब अचानक…इतना कुछ बिखर गया है मनु…मेरे मानसिक कष्ट और बीमारी तो है ही, घरेलू परेशानियाँ भी इतनी हैं कि लगता नहीं है कि अब इस भँवर से कभी निकल पाऊँगा। आपको बताऊँ, कभी-कभी लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है—कोई अनिष्टकारी व्यक्तित्व…और मैं बचूँगा नहीं। पहले भी शायद दो-एक बार मैंने आपको बताया है। जब मैं बीमार नहीं था, तब भी यह हालत थी और बीमारी के दौरान तो हर दिन यही लगता था कि यह मेरा अंतिम दिन है और अब बचना नहीं है। मनु, सचमुच मुझे समझ में नहीं आता कि मैं जीवित कैसे हूँ। जो मेरे हालात और परिस्थितियाँ है, उनमें मुझे कायदे से जीवित नहीं होना चाहिए था।”
“यानी बीमारी के कारण ही आपकी यह हालत नहीं है—आप पिछले काफी समय से ऐसा महसूस कर रहे थे।” मैंने पूछा।
अब मटियानी जी थोड़ा सुर में आए। बात के सिरे को एक लेखक के रूप में अपने स्वाभिमान और त्रासदी से जोड़कर बोले, “मैंने बताया आपको कि जो त्रासदी मैं लेखक के रूप में महसूस करता हूँ, कहीं न कहीं यह उसी की परिणति है—और यह मैं अभी नहीं, शुरू से महसूस करता आ रहा हूँ। यह अलग बात है कि व्यक्तिगत यंत्रणाएँ या पारिवारिक समस्याएँ कितनी ही ज्यादा क्यों न रही हों, इससे मेरे लिखने में कोई दिक्कत पहले कभी नहीं आई। मैंने खराब से खराब हालात में भी लिखा, लेकिन इधर पिछले पाँच-छह सालों से असलियत यह है कि मैं कुछ भी लिख सकने की हालत में नहीं रहा हूँ।”
कुछ रुककर बात को आगे बढ़ाते हुए वे बोले—
“एक विडंबना और है मनु, और यह बड़ी विचित्र है, जिसे आप शायद समझ सकें। वह यह कि इससे भी पहले मैंने लिखा तो सही, और अपने हिसाब से अच्छे से अच्छा लिखा, लेकिन जो मेरे गहरे अनुभव थे, उन्हें मैं छोड़ता गया। मन में कहीं यह बात थी कि आगे चलकर एक बड़ा उपन्यास लिखना है या कि आत्मकथा लिखनी है। पर इन चार-छह सालों में हुआ यह कि पारिवारिक झंझटों के कारण मैं कुछ भी लिख सकने में असमर्थ हो गया। लेख तो लिखे गए, लेकिन कहानी लिखने का साहस मैं नहीं जुटा पा रहा हूँ—इसलिए कि लेख तो (सिर की ओर इशारा करते हुए) ऊपर-ऊपर से लिखे जा सकते हैं, पर कहानी के लिए बहुत भीतर डूबना पड़ता है। वह हो नहीं पा रहा है। यानी आप कह सकते हैं, घरेलू परेशानियों और अपने मानसिक कष्टों के कारणों जो मुझे लिखने के लिए समय या मुक्ति चाहिए थी, वह मुझे नहीं मिल पा रही है।…तो अब मुझे दुख इस बात का है कि जो मेरे सबसे कीमती अनुभव थे, वे तो लगभग बेकार ही चले गए…और मैं कह नहीं सकता कि उन्हें कभी रचनात्मक रूप दे भी सकूँगा या नहीं। अभी तक सिर्फ निराशा ही है। देखिए, क्या होता है!”
यह सुनते ही राजेंद्र यादव का ‘न लिखने का कारण’ लेख मुझे याद आया, जो ‘हंस’ के संपादकीय के रूप में छपा था और इस पर तमाम चर्चाएँ और बहसें शुरू हो गई थीं। “क्या यह वही समस्या है, राजेंद्र यादव जिसे ‘न लिखने का कारण’ कहते हैं? या कोई भिन्न चीज…?” मैंने जानना चाहा।
पर स्पष्ट ही, मटियानी जी की दुविधा और मुश्किल कुछ अलग थी। उसे शब्दों में तहाते हुए वे बोले—
“मनु, इधर मेरे न लिख पाने की जो समस्या है, वह वही है जिसका जिक्र मैंने बरसों पहले अपने निबंध ‘लेखक की हैसियत से’ मैं किया था। इसलिए अब लिखने या न लिखने को जो तर्क है, वह मुझे कहीं अपने भीतर से ही खोजना होगा। हालाँकि यहीं एक बात मुझे और कहनी है और यह बात किसी को भले ही विचित्र लगे, पर है सच कि मेरे जीवन की जो भी विडंबनाएँ हैं—चाहे व्यक्ति की हैसियत से या लेखक की हैसियत से, उनका सामना करने का भी सिवाय लिखने के, मेरे पास कोई उपचार नहीं है। मुझे लिखना आता है तो मैं लिख ही सकता हूँ, लिखने के सिवा तो कुछ कर नहीं सकता। और यह बात घोर आर्थिक संकटों के समय भी मुझे भरोसा देती रही। मान लीजिए, जेब में थोड़े से ही पैसे हैं और उनसे सब्जी लेकर आया, जेब खाली हो गई। तो उस सब्जी वाले पर कहानी लिखी और फिर जेब में चार पेसे आ गए!…ऐसे ही घर में एक बार बिल्ली पाली। वह बहुत दूध पी जाती थी। पत्नी इस बात से चिढ़ती थी कि अब इसके लिए कहाँ से दूध का इंतजाम करें? तब मैंने…आपको यकीन नहीं आएगा, बिल्ली पर ही कहानी लिखी थी और उससे काफी अच्छे पैसे मिले थे।”
कहते-कहते मटियानी जी हँसने लगे। एक मुक्त, निर्मल हास्य, जिस पर विषाद की कोई छाया नहीं थी। बोले, “मैं तो लेखक हूँ, जिस चीज पर खर्च करूँगा, वहीं से कहानी भी निकालूँगा और पेट भरने के लिए चार पैसों की जुगाड़ कर लूँगा।”
फिर अपने अतीत में गहरा गोता लगाकर वे बंबई जा पहुँचे और बेहद कष्टों भरे अपने गर्दिश के दिनों को याद करने लगे, जब वे एक चाट की दुकान पर काम करते थे। यह सब हमारे लिए अकल्पित और अचरज भरा था। पर मटियानी बड़े सहज भाव से बताते जा रहे थे। बोले—
“मैंने जब बंबई की अपनी नौकरी छोड़ी—वहाँ एक छोटी सी चाट की दुकान में मैं नौकरी करता था—तो ‘धर्मयुग’ के संपादकीय विभाग से नंदकिशोर मित्तल ने आकर पूछा—अब क्या करोगे? इस पर मेरा जवाब था कि, खेती करूँगा। वे हैरान थे कि बंबई में तुम्हें कहाँ इतनी जमीन मिल जाएगी खेती करने के लिए? तो इस पर मैंने जवाब दिया कि मैं जमीन पर नहीं, कागज पर खेती करूँगा। वही अब तक करता भी आ रहा हूँ, मनु। अब आगे का तो कह नहीं सकता।”
कहते-कहते वे थोड़े उदास हो जाते हैं।
मटियानी जी अस्वस्थ होने से पहले एक बड़ा उपन्यास लिखने की बात सोच रहे थे। पर फिर बीमारी के कारण जैसे सब कुछ अस्त-व्यस्त-सा हो गया। जीवन ठहर सा गया। उस उपन्यास का उन्होंने कई बार मुझसे जिक्र किया था। उसी की ओर इंगित करते हुए मैंने पूछा, “आप जिस बड़े उपन्यास की बात कर रहे हैं, वह आप लिखते तो कैसा होता? और क्यों उसे लिखने की इतनी उत्सुकता आप में है?”
सवाल सुनकर मटियानी जी एकाएक उत्साहित हो जाते हैं। कुछ-कुछ अपने पहले वाले सुर में आकर उन्होंने जवाब देना शुरू किया, और न जाने कब एक अद्भुत इंटरव्यू शुरू हो गया। मटियानी जी बताने लगे—
“असल में मनु, मेरा सोचना यह है कि अब तक जो उपन्यास मैंने लिखे हैं, उनमें मुझे जूझना नहीं पड़ा। यानी ऐसा नहीं कि वे तल्लीनता से नहीं लिखे गए, पर वे मेरे लिए ऐसे थे, जैसे बच्चों का खेल हो। हद से हद पंद्रह-बीस दिन या महीने भर में उपन्यास लिखकर मैंने छपने दे दिया। अकसर मेरे साथ यही हुआ! और उसके पात्र, स्थितियाँ, परिवेश चाहे कैसा भी हो, लेकिन मेरे लिए इस कदर चुनौती भरा नहीं था कि मुझे अपनी सारी शक्ति और ऊर्जा के साथ जूझना पड़ा हो।…मैंने आपसे शायद पहले ही कई बार कहा है मनु, कि बड़े उपन्यास के बारे में मेरी दृष्टि यह है कि उसमें कथानक ऐसा होना चाहिए जिसमें लेखक को बुरी तरह जूझना पड़े। तभी बड़ी रचना संभव है। और यह जूझना ऐसा है कि आप कहाँ बैठे हैं या कहाँ पड़े हैं, क्या खा-पी रहे हैं, कुछ भी होश आपको न हो। पर मेरे जिन उपन्यासों की बहुत चर्चा भी होती है या आपको जो पसंद है, ‘बावन नदियों का संगम’, ‘मुठभेड़’, ‘गोपुल गफूरन’ वगैरह, उन्हें लिखते समय भी मुझे कुछ खास जूझना पड़ा हो, ऐसा नहीं!”
पर इधर उनकी कल्पनाओं में हर पल तैरने वाला यह बृहद् उपन्यास कुछ अलग था। भला क्यों? खुद मटियानी जी से सुनिए—
“मनु, एक बड़ा उपन्यास मुझे लिखना है—यह सपना तो मेरा बहुत पहले से था और उसके लिए जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा है, अपने बहुत से कीमती अनुभव मैं बचाकर रखता जाता थाकि वह उपन्यास लिखा गया तो ये उसमें काम आएँगे।…और फिर यह जो एक धुँधली सी कल्पना थी, कुछ आगे चलकर एक पक्के इरादे में बदल गई। उसके पीछे एक घटना है—जिसे आप चाहें तो घटना कह सकते हैं, नहीं भी!…असल में हुआ यह कि बरसों पहले मैं खंडवा जाने के लिए ट्रेन से सफर कर रहा था। रास्ते में किसी जगह एक प्रचंड आँधी सी आई। मनु, मैं ठीक-ठीक बता नहीं सकता कि वह अनुभव कैसा था। मुझे ऐसा लगा था कि जैसे वह आँधी पूरी की पूरी मेरे भीतर से गुजर गई हो।…यानी बाहर एक आँधी है, एक भीतर और दोनों की एक ही लय बन रही है। उन दिनों मैं घरेलू स्थितियों से बहुत परेशान और मर्माहत रहता था। तो शायद इसी कारण यह लगा हो कि उस आँधी का एक बड़ा हिस्सा मेरे अंदर समा गया है। यह कोई छह वर्ष पहले की बात है। एक बड़े उपन्यास का खयाल भी तभी आया और उसी क्षण मैंने उसका नाम भी रख लिया था, ‘मरुत’।”
फिर अपने इस अनलिखे महत्वाकांक्षी उपन्यास की कथावस्तु भी उन्होंने बताई। मोटे तौर से ‘मरुत’ के केंद्र में एक परिवार की कहानी है जो अपनी आंतरिक कष्टों के साथ-साथ परिस्थितियों के दबाव में जी रहा है, और उसके कारण उस परिवार के सदस्यों में किस तरह का विचलन आता है, उसके प्रवाह में मनुष्य कैसे प्रवाहित होता है—यह सब मटियानी जी दिखाना चाहते थे। उस परिवार में एक लड़के की हत्या हो जाती है। उसके बाद कानून की लड़ाई शुरू होती है और वह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। देश के कानून की जो हालत है, जो अपराधी को हर तरह की छूट देने वाली और यातनाग्रस्त को यातना देने वाली है, वह इसमें कई स्तरों पर खुलकर आती है।”
मटियानी जी का यह उपन्यास अगर लिखा जाता, तो यह बहुत कुछ आत्मकथात्मक उपन्यास होता। उनसे मैंने कहा, तो सहज ही इस बात को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा—
“हाँ, आप कह सकते हैं…! और हो सकता है, मेरे जीवन का सारा इकट्ठा हुआ अनुभव इसमें आए। मैं आपसे मनु, कई बार कहता था कि जैसे नियति मेरा पीछा कर रही है। तो वह यही है जिसे इस उपन्यास में मैं लाना चाहता हूँ। मैं अखबारों में पहले इस तरह की घटनाओं या हिंसा के बारे में पढ़ता था। मेरे मन में तभी से हौल पैदा हो गया था और कानून की हालत इस देश में जो है, वह तिलमिला देने वाली है। गोष्ठियों में अकसर मैं यह बात कहता ही था कि देश में कानून की हालत ऐसी है कि वह खुलेआम अपराधियों को बचाने का काम कर रहा है। और तो और, उसका मकसद भी यही है, चाहे वह छिपे तौर से प्रकट होता हो! यह बात मैंने—आपने पढ़ा ही होगा, ‘मुठभेड़’ में तथा ‘बावन नदियों का संगम’ में भी उठाई है, पर वहाँ वह पूरी तरह से नहीं आई। उसी को मैं बड़े उपन्यास में उतारना चाहता हूँ अगर वह लिखा गया तो! वैसे, इसकी अब बहुत ही कम संभावना बची है…तो भी अभी पूरी तरह निराश तो मैं नहीं हुआ हूँ।”
[5]
मटियानी जी जब इस आत्मकथात्मक उपन्यास की चर्चा कर रहे थे, तो मेरे भीतर कुछ और चल रहा था। मुझे बार-बार याद आ रहा था कि कुछ समय पहले तो वे अपनी आत्मकथा लिख रहे थे, ‘बंबई : खराद पर’। ‘हंस’ में उसकी कुछ किस्तें छपी भी थीं, और पाठकों ने भी उसे बेहद पसंद किया था। मटियानी जी जब बंबई में थे, तो उनकी उम्र होगी कोई बीस-बाईस बरस। वे उस तरुणावस्था में अपने घर से बंबई क्या सोचकर गए थे? क्या सिर्फ काम की ही तलाश थी या फिर कोई और धुन…? उनके भीतर कौन सा सपना था, जो उन्हें बंबई ले गया?
पूछने पर वे कहते हैं, “कुछ निश्चित नहीं था, इसलिए कि मनु, मेरी दिक्कत यह है कि जब मैं अपने जीवन के पन्ने पलटता हूँ, तो लगता है बहुत योजना बनाकर काम करने में तो मेरा कभी यकीन ही नहीं रहा। जिधर रास्ता मिला, उधर चल पड़ा वाली हालत थी। तो मोटे तौर से तो काम तलाशने की ही इच्छा थी। बंबई बड़ा नगर था तो कुछ न कुछ काम-धाम मिल ही जाएगा, कोई न कोई जुगाड़ हो जाएगा, यही सोचकर शायद घर से निकला होऊँगा। लेकिन लेखक होने की इच्छा से घर से नहीं चला था, यह भी कैसे कहूँ? इसलिए कि तब तक मैंने खूब लिखना शुरू कर दिया था और मेरी रचनाएँ पत्र-पत्रिकाओं में छपने भी लगी थीं।…तो जहाँ तक मेरा खयाल है, सिर्फ काम की तलाश में भी मैं बंबई नहीं आया था, जीवन का या लेखक के रूप में जीने का कोई रास्ता खोजने की इच्छा भी कहीं न कहीं मन में रही होगी। मैं तो—आपको बताऊँ, उस समय आजीविका के लिए हर तरफ हाथ-पैर मार रहा था। मिलिट्री में भारती होने के लिए भी गया था और वहाँ संयोगवश मैं रह गया। अगर भरती हो जाता, तो अब तक नौकरी के बाद रिटायर भी…(हँसते हैं) बहरहाल, लिखते हुए भी अब कोई पैंतालीस-छयालीस वर्ष हो गए। सन् 50-51 के आसपास छपना शुरू हो गया था।”
शुरू में मटियानी जी रमेश मटियानी ‘शैलेश’ नाम से लिखते थे, फिर वे शैलेश मटियानी हुए। मुझे लगता है, उनकी कहानी का सारा मर्म रमेश मटियानी ‘शैलेश’ से शैलेश मटियानी बनने में है। इसलिए कि उन्होंने सिर्फ नाम ही नहीं बदला, नाम के साथ ही खुद को और जीवन को देखने का समूचा नजरिया भी उनका बदल गया और फिर ऐसी टकसाली भाषा में भावार्द्र कर देने वाली ‘इब्बूमलंग’, ‘अहिंसा’, ‘छाक’ और ‘अर्द्धांगिनी’ सरीखी महाकाव्यात्मक कहानियाँ उन्होंने लिखीं, जिनके आगे ठहर सकने वाली कहानियाँ पूरे हिंदी कथा-साहित्य में नहीं हैं। पर वे रमेश मटियानी ‘शैलेश’ से शैलेश मटियानी हुए कब और कैसे? यह खुद-बुद तो भीतर थी ही। वे सामने हों, तो भला उनसे यह पूछने का लोभ संवरण कैसे हो सकता था?
सवाल पूछा गया तो जवाब में मटियानी जी की एक मुक्त और प्रसन्न हँसी देखने को मिली। एकदम अकुंठ। बोले, “असल में पहले आप को पता ही है, उस समय उपनाम लिखने की परंपरा थी। लेखक अपना उपनाम रखते थे और नाम के साथ जोड़ते थे। तो ‘शैलेश’ मैंने शायद इसलिए जोड़ा होगा कि इससे पहाड़ का बोध होता था। कुछ आगे चलकर रमेश मटियानी ‘शैलेश’ नाम अटपटा लगने लगा तो इसे सीधा कर लिया—शैलेश मटियानी। और तब से यही चला आता है।”
तभी अचानक एक अलग सा सवाल मन में कौंधा। क्या बचपन में मटियानी जी को पता था कि वे बड़े होकर लेखक बनेंगे और इतना यश कमाएँगे? और वे कौन-से हालात थे जिन्होंने उन्हें लेखक बनाया? क्या घरेलू या निजी परिस्थितियों का भी इसमें योगदान रहा? पूछने पर मटियानी जी मानो छलाँग लगाकर अपने बचपन के दिनों में जा पहुँचे। उन्होंने बड़े भावपूर्ण लहजे में कहा—
“बिल्कुल शुरू की बात करें तो…यानी एकदम छुटपन की जो तसवीर अपनी ध्यान में आती है, उसमें यह था कि कहानियाँ सुनने का मुझे बड़ा चाव था। दादी से मैं कहानियाँ सुना करता था और इतनी उत्सुकता इन कहानियों की रहती थी कि मैं आपको बता नहीं सकता।…खैर, तब तो मनु मैं यह सोच ही क्या सकता था कि मुझे आगे चलकर लेखक बनना है—या लेखक भी कोई चीज होती है जो इन कहानियों को लिखता है, यह सब सोचने की फुर्सत ही कहाँ थी? पर अब मैं उन सारी स्थितियों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि मेरे लेखक बनने की तैयारी तभी से हो गई थी।”
और फिर एक ऐसी घटना उन्हें याद आई, जिसने उन्हें भीतर-बाहर से बदल दिया। मटियानी जी उस समय बहुत छोटे ही थे। यही कोई-तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ते होंगे। जब वे गाँव में मिडिल की पढ़ाई पूरी करने अल्मोड़ा गए, तब वहाँ नगरपालिका का एक पुस्तकालय था जहाँ काफी साहित्यिक किताबें थीं। पत्रिकाएँ भी आया करती थीं। बहुत-से लेखकों को उन्होंने तभी पढ़ा। इनमें यशपाल, अश्क वगैरह थे, देवेंद्र सत्यार्थी भी थे जिनकी ‘धरती गाती है’, ‘बेला फूले आधी रात’ जैसी कई किताबें वहाँ थीं। इन किताबों, पत्रिकाओं को वे पढ़ते थे तो खुद उनकी लिखने की इच्छा होती थी। उनके आसपास एक लड़का लिखता था और उसकी कविताएँ वहाँ के एक लोकल अखकार में छपती थीं। जब उन्होंने कहा कि मैं भी लिखता हूँ तो पता चला कि संपादक ने बड़ी हिकारत से अपने मित्रों से कहा था, “अच्छा, अब बूचड़ों-कसाइयों के लड़के भी कविता-कहानियाँ लिखेंगे?”
बात मटियानी जी को चुभ गई और उन्होंने तब तय कर लिया कि अब तो लेखक बनकर ही दिखाना है। उन्होंने उस लोकल परचे में अपनी रचनाएँ भेजने के बजाय कहानियों की पत्रिका ‘रंगमहल’ में अपनी कहानी भेज दी। ‘रंगमहल’ कहानियों की बहुत अच्छी न सही, पर ठीक-ठाक पत्रिका थी और नगरपालिका के पुस्तकालय में आया करती थी। रचना भेजने के कुछ ही समय बाद उन्हें एक पोस्टकार्ड मिला जो उनके नाम कहीं बाहर से आने वाला पहला पत्र था। उसमें उनकी रचना की स्वीकृति की सूचना थी और लिखा था कि वे उनके लिए हर महीने दो कहानियाँ लिख भेजा करें।
यह उनके जीवन के कभी न भूलने वाले यादगार पलों में से एक है। उस पल मटियानी जी की भावाकुलता कैसी थी, इसे उनके शब्दों में ही सुनें, “अब इस पत्र को पाकर मेरी क्या हालत हुई होगी मनु, आप मुश्किल से ही कल्पना कर सकते हैं। मैं लगभग बावला ही ही हो गया था। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि यह पत्र मेरे नाम ही आया है और फिर तो हालत यह कि मैं पानी भरने जा रहा हूँ तो चुपके से निकालकर उसे पढ़ लिया। बाजार गया तो फिर चुपके से पढ़ लिया…जंगल में गया तो फिर चुपके से निकालकर पढ़ लिया। यहाँ तक कि रात को सोया तो टार्च पास रहती थी, आधी रात को उठकर फिर से पढ़ लिया कि…”
“अक्षर कहीं उड़ तो नहीं गए…!” मटियानी के अधूरे वाक्य को पूरा करते हुए मैंने कहा। सुनकर वे बड़ी जोर से हँसे। बोले, “हाँ, बिल्कुल!…यही हालत थी।”
बरसों तक वह पोस्टकार्ड मटियानी जी के पास रहा और उन्हें बचपन के उसी भावनात्मक प्रकंप और उत्तेजना की याद दिलाता रहा। बाद में वह कहीं गुम हो गया और उन्हें उसके गुम होने का उन्हें बड़ा अफसोस था। मटियानी जी ने बहुत भावुक होकर कहा, “वह मेरे लेखक होने का पहला अहसास था और मेरे लिए वह किसी चमत्कार से कम नहीं था।”
लेखक की रचना छपने पर उसे इसका पारिश्रमिक भी मिलता है, इसका तो उन्हें खयाल ही नहीं था और तब ये सारी बातें वे सोच भी क्या सकता थे? रचना छप गई, इससे बड़ा सुख और कोई न था। पर फिर पहला पारिश्रमिक मिला, तो उनकी हालत क्या हुई, यह भी जरा मटियानी जी से ही सुनें—
“अलबत्ता पहला पारिश्रमिक मुझे एक कहानी का मिला था—आठ रुपए। उन दिनों आठ रुपए कम नहीं होते थे। फिर मेरे जैसे आदमी के लिए तो वे इतने ज्यादा थे कि आप समझ लीजिए, जब डाकिए ने मुझे रुपए दिए और दस्तखत करने के लिए कहा तो उत्तेजना के मारे मेरे हाथ काँप रहे थे। जो आठ रुपए डाकिए ने मुझे दिए, उसमें से एक रुपया मैंने उसे दे दिया…और ये सात रुपए मेरे जेब में पड़े हुए ऐसे लग रहे थे, जैसे मैंने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना हासिल कर लिया हो।”
मटियानी जी की ये शुरुआती कहानियाँ कहीं इधर-उधर हो गईं। इसलिए किसी संग्रह में नहीं आईं। पर ये कहानियाँ बड़े मन से लिखी गई थीं और उन्हें निस्संदेह प्रिय थीं। लिहाजा वे कहे बगैर नहीं रहते कि “वे मेरे पास होतीं तो मैं उन्हें जरूर शामिल करता।”
[6]
‘सारिका’ का ‘गर्दिश के दिन’ स्तंभ बड़ा चर्चित और पठनीय था। उसमें बहुत से लेखकों के ‘गर्दिश के दिन’ छपे थे, जिनमें मटियानी जी भी थे। एक तरह से उनके गर्दिश के दिनों की करुण व्यथा सबसे मार्मिक और स्तब्ध कर देने वाली थी। पर उनके ‘गर्दिश के दिन’ औरों से इस मानी में अलग थे कि उन्होंने अपने बुरे दिनों को कोसा नहीं है, बल्कि एक तरह की कृतज्ञता ही प्रकट की है। इसलिए कि उन्हें लगता था कि ये गर्दिश के दिन मेरे लिए तो सही मायने में ‘अग्निपरीक्षा’ के दिन हैं। आखिर इसी से गुजरकर ही तो वे एक लेखक होने की सच्ची अनुभूति और विश्व-करुणा हासिल कर पाएँगे। मटियानी ने बड़ी गहरी संवेदना में डूबकर बताया—
“यह बात तय थी और कम से कम मेरे मन में तो यह पक्के तौर से बस गई है—कि अगर मैंने इतने अपमान और तकलीफें न झेली होती तो जो कुछ मैं लिख पाया, न लिख पाता या जिस कद का लेखक मैं बना, न बन पाता। इसलिए उन दुखों और कष्टों के लिए मन में घृणा का भाव होने का तो सवाल ही नहीं। और दूसरी बात यह कि चाहे मुझे एक से एक खराब स्थितियाँ झेलनी पड़ीं, लेकिन तो भी इतना तय है कि मुझे उन गरीब, असहाय, भूखे लोगों में—यहाँ तक भिखारियों और कँगले लोगों तक में इतने एक से एक अच्छे लोग मिले कि मेरा मन अब भी उनके प्रति कृतज्ञता से भरा हुआ है और जीवन भर रहेगा। उन मैले-कुचैले लोगों, कोढ़ियों और भिखारियों में मुझे जो मनुष्यता नजर आई, वह आज के सभ्य और शालीन लोगों में शायद ही कहीं मिले।”
यह बात कहते हुए उन्हें अल्मोड़े की एक घटना याद आ गई। उसका जिक्र करते हुए वे बोले—
“उन दिनों में एक कसाई की दुकान पर कीमा काटने का काम किया करता था। कविताएँ लिखना भी मैंने शुरू कर दिया था और वे जहाँ-तहाँ छपने भी लग गई थीं। तो उन्हीं दिनों की बात है। शाम का समय था, मैं कीमा काटने के काम में लगा हुआ था। इतने में ही दो-तीन लोग सड़क पर बातचीत करते हुए निकले। उनमें से एक ने मेरी ओर देखते हुए व्यंग्य से कहा—देखो, सरस्वती का कीमा काट रहा है! और ऐसा कहकर उसने सड़क के किनारे थूक दिया।…मेरे हाथ वहीं रुक गए और मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं ऐसा कहने वाले आदमी की छाती में चाकू घोंप दूँ। तब मैं कसाई की दुकान पर काम करने के साथ-साथ नवीं क्लास में पढ़ता था और कविताएँ लिखने भी लगा था। भावुक बहुत था।…मुझे अब भी याद है, उस रात मैं दीवार से सिर पटक-पटककर रोता रहा था और मन ही मन एक ही प्रार्थना कर रहा था कि हे सरस्वती माँ, तू मुझे चाहे कितने ही कष्ट दे देना, पर मुझे लेखक जरूर बनाना।”
एक क्षण की मौन निस्तब्धता के बाद उन्होंने कहा, “आज यह बात किसी को अजीब लग सकती है, पर मैं सचमुच इतना ही भावुक था, इसीलिए कष्टों से मैं घबराता नहीं। आज भी कहीं न कहीं यह बात मेरे भीतर बैठी हुई हैं कि कोई लेखक जितने कष्ट सहता है, उतना ही बड़ा उसका लेखन होता है। और यह भी शायद नियति का कोई चमत्कार ही है कि कष्ट मुझ पर कितने ही आए हों, रास्ता भी कोई न कोई हमेशा निकलता ही गया। यहाँ तक कि ऐसा भी हुआ कि घर में दाने नहीं हैं, पूरे परिवार के भूखों मरने की नौबत आ गई। फिर कहीं न कहीं कुछ हुआ और गाड़ी चल निकली। बस, आखिरी कुछ बरसों में ही यह क्रम लडख़ड़ाया…और मेरे मानसिक कष्टों की शुरुआत भी तभी से हुई।”
[7]
अरसे से मटियानी जी के साथ रहते-रहते इतना तो जान ही लिया था कि वे कोई कोई बौद्धिक मुद्राओं वाले नकचढ़े कहानीकार नहीं हैं, जिन्हें लिखने के लिए कहीं दूर मनोरम एकांत स्थलियों में जाना पड़े। तो भी यह जिज्ञासा तो मन में थी ही कि आखिर उनका लिखने का ढंग क्या है? क्या वे अपने लिखे हुए को बार-बार काटते और माँजते हैं? और फिर कहानी या उपन्यास लिखने का उनका मूड कैसे बनता है? यह सवाल भी बार-बार जेहन में आ रहा था।
पूछने पर उनका जवाब बड़ा दिलचस्प था, “देखिए, ज्यादातर तो मैं अपनी कहानियों का एक ही ड्राफ्ट लिखता हूँ। दूसरा ड्रॉफ्ट बनाने की मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। और आपको आश्चर्य होगा, मेरी ज्यादातर कहानियाँ एक या दो बैठकों में ही पूरी हो जाती हैं—ज्यादा से ज्यादा कोई कहानी जो या तीन चलती है, लेकिन यह भी कम, बहुत कम होता है। वरना तो मेरी ज्यादातर कहानियाँ एक ही सिटिंग में लिखी गई हैं और लिखते समय मनु, आपने भी महसूस किया हो और मैंने तो अनेक बार महसूस किया है कि बिल्कुल शास्त्रीय संगीत की तरह कहानियों की भी एक ऐसी लय सी बन जाती है और शब्द खुद-ब-खुद उस लय से ढलते चले जाते हैं…कि फिर आप कहानी नहीं लिखते, जैसे कोई और ही है, जो आप से लिखवाता चल रहा हो।”
और आश्चर्य! लिखते समय मटियानी जी की ऐसी लय एक बार बन जाए तो फिर आसपास कितना ही शोर हो रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक बार मन में धुन आ जाए कि लिखना है तो फिर मूड बनाने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती थी। खुद मटियानी जी के शब्दों में—
“कई बार तो यह भी हुआ कि पड़ोस में कहीं जागरण है और रात भर शोर मच रहा है या फिर बच्चों की चिल्ल-पों, आने-जाने वालों की व्यस्तता, लेकिन इस सबके बावजूद मैं लिखता रह सकता हूँ। बस, शर्त यह है कि मेरा चित्त शांत होना चाहिए। चित्त में शांति हो तो मैं घोर अशांति और दारिद्रय में भी, जहाँ मामूली सा एकांत या शांति भी न हो, और घर में कल के लिए आटा तक न हो, लिखता रह सकता हूँ। ज्यादातर मेरी कहानियाँ कितनी दारुण यंत्रणाओं के बीच लिखी गई हैं, लोगों को इसका अनुमान नहीं है। अब ‘अर्धांगिनी’ कहानी को लें, जो मूलत: पारिवारिक प्रेम की कहानी है। इसकी लय संगीतात्मकता को लोगों ने खूब पसंद किया है। लेकिन आपको बताऊँ, सुप्रीम कोर्ट में मैं मुकदमा हार गया था। उस दुख और तनाव से मुक्ति पाने के लिए मैंने यह कहानी लिखी थी।”
“आश्चर्य है, कहानी में इसकी छाया तक नहीं है!” सुनकर एक प्रसन्न हँसी के साथ मटियानी जी कहते हैं, “अब देख लीजिए आप…!” इसके साथ ही उन्होंने एक नई जानकारी और दी। मुझे थोड़ा विस्मित करते हुए उन्होंने कहा—
“ज्यादातर तो मैं अपनी रचनाओं में काट-छाँट नहीं करता। पहली बार में जो रूप बना, वही छपने भेजता हूँ। और यह बात कहानियों में नहीं, उपन्यासों में भी लागू होती है। उनका भी मैं एक ही ड्राफ्ट तैयार करता हूँ और वही मेरा पहला और अंतिम ड्राफ्ट होता है। पर कई बार ऐसा भी हुआ कि बरसों बाद मैंने अपनी रचनाओं में संशोधन किया। जैसे ‘बर्फ गिर चुकने के बाद’ का नया संस्करण आया तो मैंने इसे फिर से संशोधित किया। इस बारे में मेरा मानना है कि आप अगर अपनी रचना से संतुष्ट नहीं है, तो हर बार नए संस्करण में आप उसे संशोधित करें, इसका पूरा अधिकार है आपको!…इस लिहाज से अपने इंटरव्यू में देवेंद्र सत्यार्थी ने लेखन को जैसे शास्त्रीय संगीत के रियाज की तरह माना है, मेरा भी यही मानना है—और सचमुच यह कमाल की उपमा है।”
इसके साथ ही एक हैरान कर देने वाली बात उन्होंने और बताई, “कहानी लिखने का मेरा ढंग यह है कि मैं कहानी शुरू करने से पहले शीर्षक लिखकर रख लेता हूँ। बगैर शीर्षक लिखे कहानी शुरू कर सकना अब तक भी मेरे लिए संभव नहीं है।”
[8]
मटियानी जी को इस बात से बड़ी तकलीफ होती थी कि हिंदी के लेखक और साहित्यकार वैचारिक असहमतियों का बुरा मानते हैं और न सिर्फ बुरा मानते हैं, बल्कि व्यक्तिगत आक्षेपों पर उतर आते हैं। चुपके-चुपके पीछ से षड्यंत्र करने, बदला लेने या तबाह कर देने की कोशिशें करते हैं। उन्होंने बहुत करुण लहजे में कहा, “मुझे इस तरह के बहुत बुरे अनुभव हैं और इसी कारण मैं कहता हूँ कि हिंदी में ज्यादातर छोटे कद के लेखक हैं जो बड़ी रचना कर ही नहीं सकते, बड़ा विचार भी नहीं दे सकते।”
दूसरी ओर, मटियानी जी के पाठक उनकी सबसे बड़ी शक्ति हैं, जिन्होंने उन्हें खुली बाँहों से अपनाया है, जबकि ज्यादातर स्वनामधन्य आलोचकों ने उनकी घोर उपेक्षा की। खुद मटियानी जी यह स्वीकार करते हैं कि “अगर मुझे पाठकों का इतना ज्यादा प्यार न मिला होता तो मैं आज शायद जीवित ही न होता! मेरे पाठक न जाने कहाँ-कहाँ से मुझे मिले और किस-किस तरह से भाव-विभोर होकर उन्होंने अपनी भावनाएँ मुझ तक पहुँचाईं, मैं आपको बता नहीं सकता। इतने लोगों के पत्र, इतने प्रशंसात्मक पत्र आते हैं…कि मैं चाहकर भी उनका संग्रह नहीं कर सका। अधिकांश पत्र तो मैंने फाड़ ही दिए हैं, लेकिन जो बचे हैं, उन्हीं को सँभालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है! इतने पाठक हैं मेरे कि मैं देश के किसी भी हिस्से में गया, मुझे अपने पाठक मिले, उनका बेशुमार प्यार और सहयोग मिला…!”
भले ही तरह-तरह की खेमेबंदी में कैद आलोचकों ने उनकी जान-बूझकर उपेक्षा की हो, लेकिन मटियानी जी को पूरा यकीन था कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा, “लेखक की हैसियत से यह विश्वास कहीं मेरे भीतर है कि अगर आप कोई बेईमानी नहीं कर रहे और रचना के पीछे आपके सच्चे और ईमानदार अनुभव हैं तो आपको दबाया नहीं जा सकता!” कहते-कहते एक फीकी, उदास मुसकराहट उनके होंठों पर नजर आई।
काश, मटियानी जी की पुरानी चमक और कड़क व्यक्तित्व फिर से लौट आए! सीढ़ियाँ उतरते वक्त हमने खुद को समवेत प्रार्थना करते पाया।…
पर दुर्भाग्य तो अपनी चाल चल रहा था। मटियानी जी से यही मेरी आखिरी मुलाकात थी। हाँ, उनके पत्र लगातार आते रहे। बहुत-बहुत लंबे-लंबे पत्र, जिसमें उनकी भीतरी चिंताएँ, उलझनें, पारिवारिक सुख-दुख और एक लेखक के रूप में पूरे स्वाभिमान से जीने की ललक कई-कई रूपों में प्रकट होती थी। फर्क बस यह होता था कि अब वे पत्र स्वयं लिखने में असमर्थ हो जाने के कारण किसी और से लिखवाकर भेजते थे। उसी दौर का उनका एक लंबा पत्र मैंने भाई ज्ञानरंजन जी को भेजा और उसे उन्होंने ‘पहल’ में अपनी टिप्पणी के साथ बड़े सम्मान से छापा था।
मटियानी जी जिस लंबी, असाध्य बीमारी की चपेट में आ गए थे, वह आखिर उन्हें साथ लेकर ही गई। पर उन्होंने इतनी अमर और कालजयी कृतियाँ हिंदी को दी हैं कि उनका यह कहना जरा भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं लगता कि “मनु, मैं प्रेमचंद के बाद खुद को हिंदी का सबसे बड़ा कहानीकार मानता हूँ।”
मुझे याद है, हिंदी भवन में हुई मटियानी जी की शोकसभा में हिंदी के कुछ दिग्गज आलोचक भी थे, जिन्होंने बड़ी शरमिंदगी के साथ कहा कि मटियानी जी सरीखे जनता के दुख-दर्द से जुड़े बड़े कहानीकार पर उन्होंने आज तक एक शब्द भी नहीं लिखा। पर अब वे उन्हे गंभीरता से पढ़ेंगे और उन पर लिखेंगे भी।…पर उन स्वनामधन्य आलोचकों ने ‘इब्बूमलंग’, ‘चील’, ‘दो दुखों का एक सुख’, ‘महाभोज’, ‘अहिंसा’, ‘छाक’, ‘माता’, ‘अर्धांगिनी’ सरीखी जनता के सुख-दुख से जुड़ी अमर कहानियाँ लिखने वालों के लिए अपनी स्याही की एक बूँद बरबाद करना भी उचित नहीं समझा। शायद इसलिए कि मटियानी अपनी जिद में जीने वाले स्वाभिमानी लेखक थे और आलोचकों की जी-हुजूरी करने से उन्हें नफरत थी।
पर मटियानी मामूली कथाकार नहीं हैं। जैसा कि बाबा नागार्जुन ने कहा, वे हिंदी के गोर्की थे, जिन्हें पाठकों का बेइंतिहा प्यार मिला था। मटियानी जी के पास जितनी उम्दा और हर लिहाज से प्रथम श्रेणी की रचनाएँ हैं, उतनी प्रेमचंद के बाद शायद ही किसी हिंदी कथाकार के यहाँ देखने को मिलें। इस लिहाज से हिंदी को कोई भी बड़े से बड़ा कथाकार उनके समकक्ष नहीं ठहरता। इसी तरह हिंदी कथा-साहित्य में रेणु की आंचलिकता की बहुत तारीफ होती है, पर जैसा कि राजेंद्र यादव जी ने भी कहा, हिंदी के आंचलिकता की शुरुआत बहुत पहले मटियानी जी अपनी कहानियों और उपन्यासों में कर चुके थे।
मटियानी जी हिंदी के बड़े और दिग्गज कथाकार ही नहीं, हिंदी कथा-साहित्य के शलाका-पुरुष हैं, जिनसे हिंदी कहानी का कद और ऊँचाई नापी जा सकती है। तो फिर उन सरीखे कथा-पुरुष को भला आलोचकों के सर्टिफिकेट की क्या परवाह? वे और उनकी कहानियाँ शताब्दियों तक पाठकों की स्मृतियों में जिएँगी। तब भी, जब तमाम नामचीन आलोचकों के नाम भी पाठकों की स्मृति से धुल चुके होंगे।
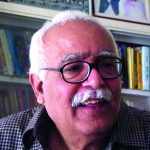
मटियानी जी की कहानियाँ एक बार पढ़ते ही पाठकों के दिलों में हमेशा-हमेशा के लिए घर बना लेती हैं और रोशनी के कतरों की तरह भीतर जगमगाहट पैदा करते हुए हमारी आस्था को संबल प्रदान करती हैं। किसी लेखक की इससे बड़ी शक्ति और अमरता भला और क्या हो सकती है!
**
प्रकाश मनु, 545 सेक्टर-29, फरीदाबाद (हरियाणा), पिन-121008,
मो. 09810602327,
ईमेल – prakashmanu333@gmail.com
============================
दुर्लभ किताबों के PDF के लिए जानकी पुल को telegram पर सब्सक्राइब करें
 जानकी पुल – A Bridge of World's Literature. जानकी पुल पर प्रकाशित लेखों में प्रकट विचार लेखक के होते हैं. उनसे मॉडरेटर का सहमत होना जरूरी नहीं है. हाँ, अपने लेखों में प्रकट विचारों के लिए मॉडरेटर खुद जिम्मेदार है
जानकी पुल – A Bridge of World's Literature. जानकी पुल पर प्रकाशित लेखों में प्रकट विचार लेखक के होते हैं. उनसे मॉडरेटर का सहमत होना जरूरी नहीं है. हाँ, अपने लेखों में प्रकट विचारों के लिए मॉडरेटर खुद जिम्मेदार है


2 comments
Pingback: officeday
Pingback: เกมยอดนิยม PRETTY GAMING